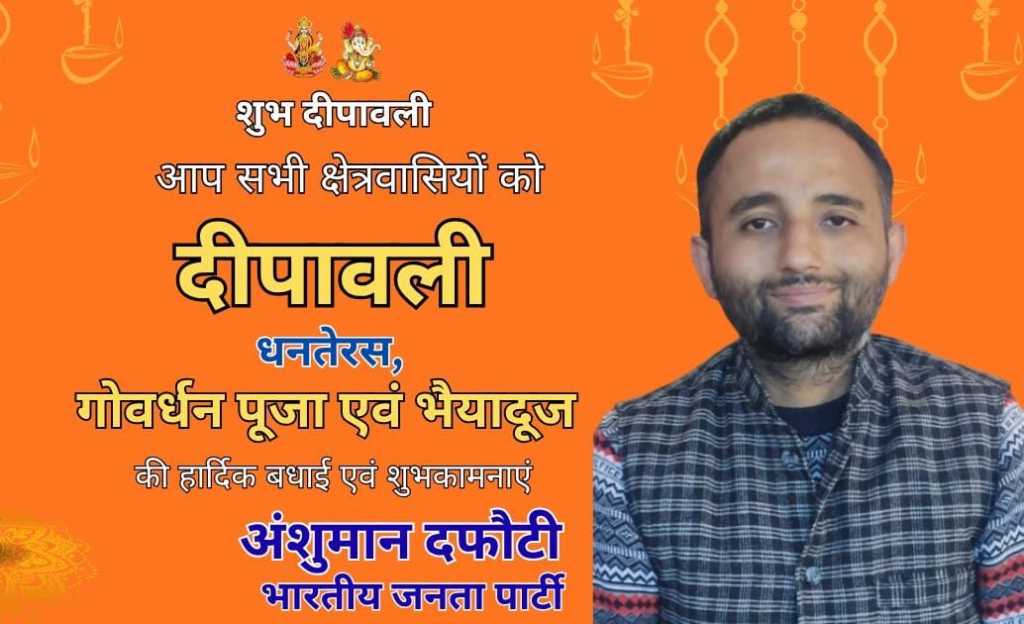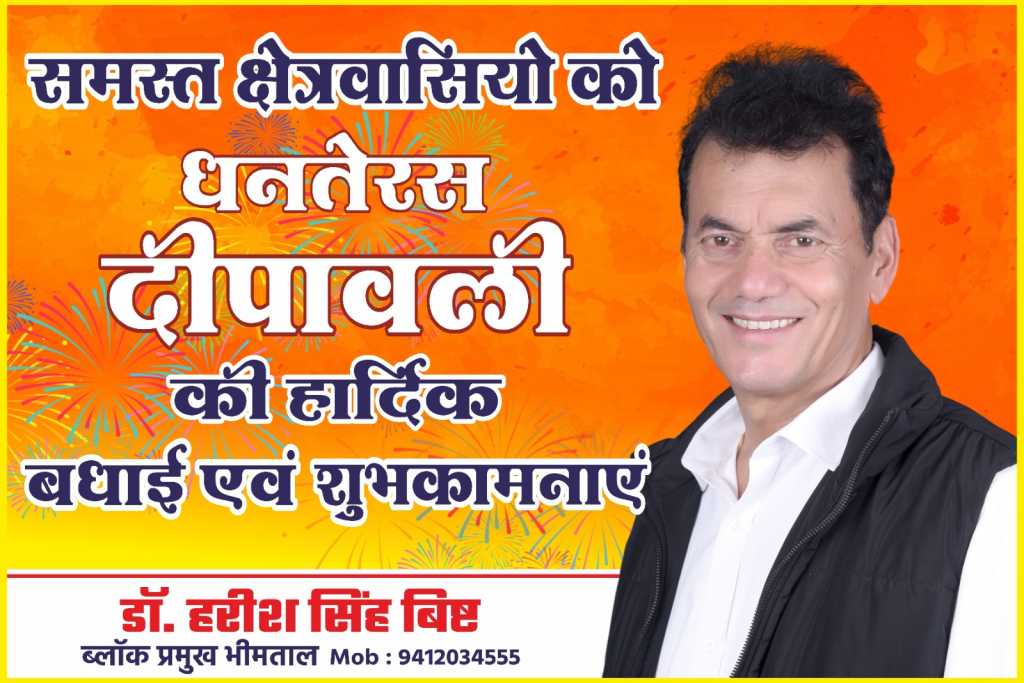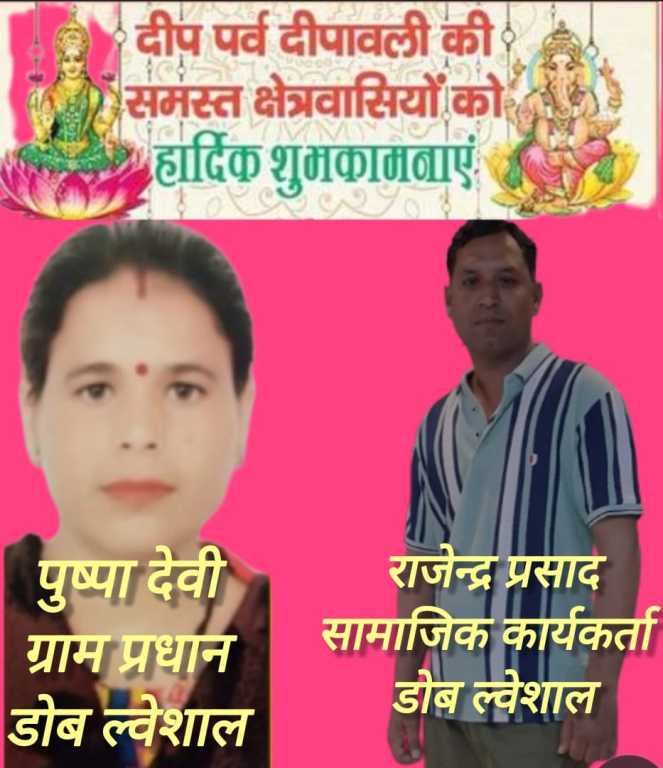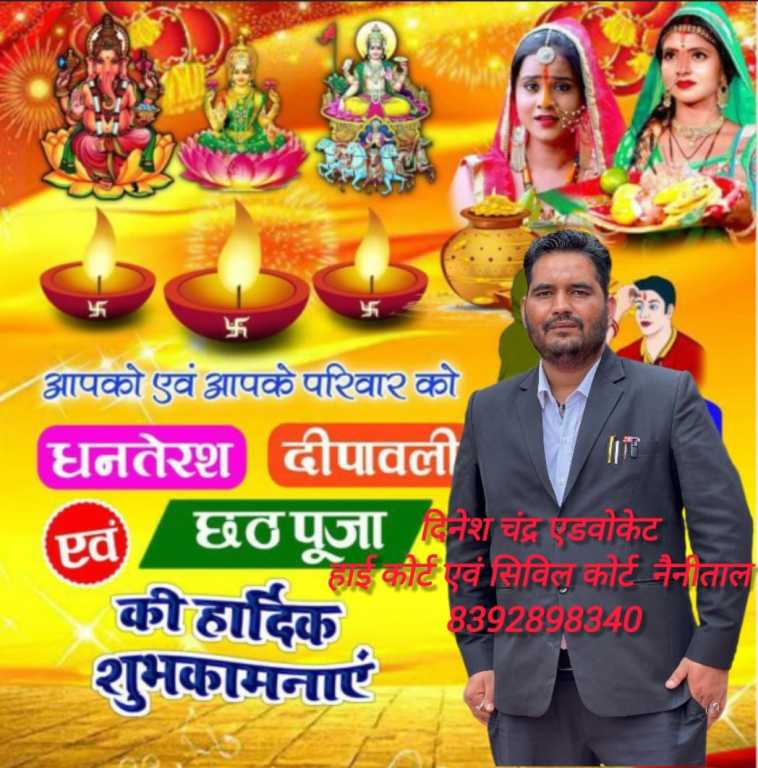नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज), जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, और दून विश्वविद्यालय, देहरादून संयुक्त रूप से 17-20 दिसंबर, 2024 के दौरान दून विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय एरोसोल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संघ (आईएएसटीए) सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहे हैं। इस सम्मलेन में वैज्ञानिक ज्ञान, हाल के शोध परिणामों और संसाधनों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 19 दिसंबर, 2024 को उत्तराखंड की वायु गुणवत्ता पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।
इस प्रतिष्ठित पैनल में शामिल थे यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, बीएआरसी के स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण समूह के निदेशक डॉ. दिनेश के अस्वल, आईआईटी बॉम्बे के प्रो. वाई.एस. मय्या, बीएआरसी के रेडियोलॉजिकल भौतिकी और सलाहकार प्रभाग की प्रमुख डॉ. (श्रीमती) बी.के. सपरा, बीएआरसी के वैज्ञानिक डॉ. मनीष जोशी और TV9 डिजिटल की सहायक समाचार संपादक सुश्री नमिता सिंह। चर्चा उत्तराखंड, विशेष रूप से देहरादून, की खराब होती वायु गुणवत्ता और इसके समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर केंद्रित थी।
किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले उसे उत्पन्न करने वाले स्रोतों की पहचान करना आवश्यक है। उत्तराखंड में प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत हैं धूल, जैवभार का ज्वलन और वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन। उत्खनन और निर्माण गतिविधियाँ धूल का मुख्य कारण हैं, जबकि जैवभार के ज्वलन में उत्तर भारत में जंगलों की आग और फसलों के अवशेष (पराली) जलाना शामिल है। इनसे उत्पन्न होने वाले अतिसूक्ष्म कण, जिन्हें एरोसोल कहा जाता है, लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है। सर्दियों के मौसम में जब अफ्रीकी और अरब क्षेत्रों से हवाएँ उत्तर भारत में अधिक एरोसोल लाती हैं, तब यह स्थिति विशेष रूप से खराब हो जाती है।
पैनलिस्टों ने भारत के भीतर सटीक उपकरण विकसित करने और उन्हें मानकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि बड़ी संख्या में समन्वित वायु गुणवत्ता मापक यंत्र बड़े शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में भी लगाए जा सकें। वैज्ञानिक समुदाय से विभिन्न प्रकार के PM2.5 को वर्गीकृत करने और उनके अंतर की जाँच करने का आग्रह किया गया क्योंकि सभी PM2.5 समान रूप से खतरनाक नहीं होते। वर्तमान में सभी PM2.5 को मापन के लिए एक ही श्रेणी में रखा जाता है।
ब्लैक कार्बन, कार्बन का एक अत्यधिक प्रदूषक रूप है, जो जैवभार जलने, जैसे जंगलों की आग, के कारण उत्पन्न होता है। यह हिमनदों पर जमा हो जाता है और सूर्यप्रकाश के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हिमनद तेजी से पिघलते हैं। चीड़ के पिरूल अत्यंत ज्वलनशील होते हैं और इस क्षेत्र में जंगल की आग का एक बड़ा कारण हैं। यदि उन्हें उर्वरकों या कम लागत वाले ऊर्जा स्रोतों जैसे अन्य उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके, तो यह कई लाभों के साथ एक बड़ी समस्या का समाधान करेगा।
पैनलिस्टों ने यह भी कहा कि आईएएसटीए एरोसोल से निपटने वाली सेवाओं या उत्पादों के मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP), मानकों और प्रमाणन में मदद करके नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक समुदाय, उद्योग और समाज के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर सकता है। दर्शकों की बातचीत ने दिलचस्प विचार उजागर किये और इस बात पर सहमति हुई कि हालांकि सम्मेलन और कार्यशालाएँ उपयोगी हैं, आईएएसटीए इससे आगे जाने की आवश्यकता है। जैसे नीति निर्माताओं की सहायता के लिए कार्य बिंदुओं की सिफारिश, उद्योगों को उनके उत्सर्जन से निपटने में मदद तथा छात्रों व जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। सभी हितधारकों को शामिल करने वाले ऐसे समावेशी कदम बहुत आगे तक जाएँगे। इसी तरह, विद्युतीय वाहनों (ईवी) के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत अनिवार्य हैं और भारत पहले से ही उस दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। अंततः पैनल ने सुझाव दिया कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कदमों का सख्ती से क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें